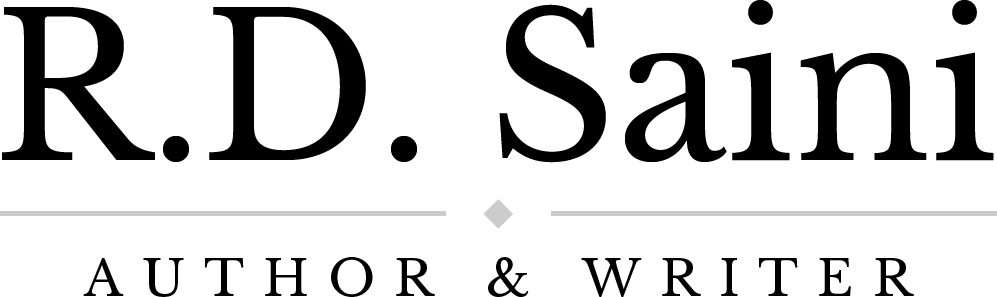सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव में हुआ था। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। विवाह के समय उनकी आयु मात्र 9 वर्ष थी। उनका विवाह जोतीराव फुले के साथ तद्कालीन समाज की रीत के मुताबिक हुआ था। यही जोतीराव फुले आगे चलकर महात्मा ज्योतिबा फुले कहलाए थे। सावित्रीबाई सच्चे अर्थ में जोतीराव की जीवन साथी बनी। उन्होंने पति के संघर्ष, उनकी जनसेवा के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया।
सावित्रीबाई ने पाया कि वे एक ऐसे नेक इंसान की धर्मपत्नी है, जो अछूतों की दुर्दशा से बहुत दुःखी एवं चिन्तित है। वे उनकी तरक्की और खुशहाली के बारे में सावित्रीबाई से चर्चा करते रहते थे। काफी सोच विचार के बाद में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बहुत सी सामाजिक बुराईयों और अछूतों की दुर्दशा का मूलकारण उनकी अशिक्षा है। महिलाओं की हालत तो और भी खराब है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को तालीम देना जरूरी समझा और यहीं से अपनी समाज सेवा के काम की शुरूआत की। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने खुद अपने पति से पढ़ना प्रारम्भ किया।
सन् 1848 में पुणे की बुधवार पेठ में जोतीराव ने अपनी कन्या पाठशाला खोली। इतिहास से पुष्टि होती है कि गैर सरकारी स्तर पर कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय जोतीराव हैं। वे खुद ही बालिकाओं को पढ़ाते थे। उनकी पाठशाला में बालिकाएं पढ़ने लगी तो पुणे के कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आया। उनकी नजर में महिला शिक्षा घोर पाप थी। जोतीराव की दृड़ता को वे जानते थे अतः उन्होंने जोतीराव को विफल करने के लिए उनके चरित्र पर कीचड़ उछालना प्रारम्भ किया। तब जोतीराव को लगा कि इस काम को जारी रखने के लिए महिला का अध्यापिका होना बहुत जरूरी है।
उस जमाने में महिला अध्यापिका की कल्पना ही सम्भव नहीं थी। जोतीराव ने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई को यह जिम्मेदारी सौंपी, जिनको वे घर पर ही पढ़ाकर इस काम के लिए तैयार कर चुके थे। सावित्रीबाई खुशी-खुशी इस काम में जुट गयीं। बाद में सावित्रीबाई ने मिसेज मिचेल के नार्मल स्कूल में अध्यापिका का निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा किया। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके व महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित अध्यापिका बनी। तब उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी। मेरी जानकारी के अनुसार वे महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि भारत की भी प्रथम प्रशिक्षित अध्यापिका कहीं जा सकती हैं।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे श्री भिड़े के मकान में प्रारम्भ की गई कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका बन गयीं। उस समय के दकियानूसी समाज की नजर में सावित्रीबाई द्वारा अध्यापन करना धर्म और समाज के विरूद्ध द्रोह करने से कम नहीं था। जब वे पढ़ाने के लिए पाठशाला आती-जाती तो उन पर फब्तियां कसी जाती, कीचड़-गोबर फैंका जाता और पत्थर तक मारे जाते। परन्तु सावित्रीबाई ने धैर्य, साहस और निडरता के साथ इन सब बाधाओं का सामना किया।
वस्तुतः जोतीराव के सान्निध्य में सावित्रीबाई समझ चुकी थी कि इस प्रकार की बाधाएं, अड़चनें और दिक्कतें कदम-कदम पर आयेंगी। यह भी वे जान चुकी थीं कि महिलाओं के उद्धार, उनकी तरक्की और खुशहाल जिन्दगी के लिए उनको शिक्षित करना जरूरी है। इसी से उनकी गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी। इसी दौरान उन्हें थामस क्लार्कसन की जीवनी पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने हब्शियों को गुलामी से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद सावित्रीबाई की यह धारणा पक्की हो गयी कि पिछड़ों, शूद्रों, गरीबों और महिलाओं को गुलामी का अहसास तब तक नहीं होगा जब तक कि वे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे।
जोतीराव फुले एवं सावित्रीबाई फुले ने दीनहीन एवं पिछड़े तबके के लोगों को शिक्षा देने का काम शुरू किया था। यह समाज के बड़े माने जाने वाले लोगों को पसन्द नहीं आया। सनातनी लोगों ने जोतीराव के पिता के कान भरे कि उनके बहू बेटे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं।
यहां गौर करने की बात यह है कि जोतीराव फुले जिस मार्ग पर अग्रसर थे वह कांटों से भरा हुआ था। उनके माली हालात भी अच्छे नहीं थे। जोतीराव फुले ने समस्त योग्ताओं के बावजूद राजकीय सेवाएं स्वीकार नहीं की थी। जाहिर है कि उनके समक्ष आर्थिक संकट निरन्तर बना रहा होगा। सामाजिक दृष्टि से भी परिस्थितियां उनके विपरीत थीं। इसकी पराकाष्ठा वहां दिखाई देती है जब जोतीराव फुले को उनके पिता ने 1849 में घर से निष्काषित कर दिया था। उनके सामने विकल्प रखा गया था कि या तो वे अपनी पाठशाला चलाना बन्द कर दें या घर छोड़ कर चले जाएं।
जोतीराव ने पाठशाला बन्द करने से इनकार कर दिया। वे अपनी पुस्तकें, कपडे़ आदि समेटने लगे तो सावित्रीबाई ने पति से पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है? जोतीराव ने कहा-‘तुम अपना निर्णय स्वंय करने के काबिल हो।’
सावित्रीबाई ने अविलम्ब निर्णय सुना दिया-‘आपने काबिल बनाया है और मैं आपसे अलग नहीं हूँ। आपके साथ चलूंगी।’
सावित्रीबाई फुले का यह निर्णय सामान्य नहीं था। उन्होंने जोतीराव फुले का वरण बाल्यावस्था में किया था तब वे अबोध थी। किन्तु इस निर्णय के समय वे समझदार थी। इस निर्णय के साथ ही मानो उन्होंने उन चुनौतियों, दिक्कतों और तकलीफों का वरण भी कर लिया जो जोतीराव से जुड़ी थीं। इस नजर से देखने पर वे एक आदर्श अर्द्धांग्निी ही नहीं बल्कि एक ऐसी नारी के रूप में दिखाई देती हैं जो अभावों और कष्टों से जूझते हुए न सिर्फ पति को ऊर्जा देने में सक्षम है अपितु उनके कार्याे में, उनके संघर्षों में बराबर की भागीदार भी है। तत्कालीन सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर इस प्रकार की दृढ़ता सावित्रीबाई फुले को एक प्रभावी प्रेरक सिद्ध करती है। इससे आगे की जीवन यात्रा में वे अपने पति के समस्त कार्यों में सक्रिय सहयोगी बनी।
सावित्रीबाई का रहन-सहन बहुत सादा था वे खद्दर के कपडे़ पहनती थी। माना जाता है कि देश में 1905-1906 से खद्दर को खास अहमियत मिली है। लेकिन इससे पहले जोतीराव और सावित्रीबाई फुले खद्दर को अपना पहनावा बना चुके थे।
सन् 1848 से 1852 के दौरान फुले-दम्पत्ति ने पिछड़े एवं गरीब तबके बालक-बालिकाओं के लिए 18 पाठशालाएं खोलीं। इन पाठशालाओं के संचालन में सावित्रीबाई ने एक अध्यापिका, प्रधानाध्यापिका एवं संचालिका के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभायी। उन्होंने इन पाठशालाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाया और उसको लागू किया।
फुले दम्पत्ति ने अछूतों की बस्ती के एक मन्दिर में पाठशाला खोली ताकि अछूतों के बालक-बालिकाओं को तालीम दी जा सके। परन्तु कुछ दिनों बाद ही छात्रों की संख्या घट गई। पड़ताल करने पर पता चला कि अछूत बच्चों के माता-पिता भयभीत थे। वे समझ रहे थे कि उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जायेगा और उनकी सात पीढ़ियों को नरक में जाना पडे़गा।
जोतीराव ने पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि यह किसी कट्टरपंथी की कारस्तानी है। ऐसे में जोतीराव ने उन बच्चों के माता-पिता को समझाया कि अब हुकूमत गोरे साहबों की है और गोरे साहबों ने कहा है कि अछूत बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे तो उनकी 14 पीढ़ियां नर्क में चली जायेंगी। इससे स्थिति सुधर गयी। परन्तु सावित्रीबाई को घर-घर जाकर अछूत बच्चों को लाना पड़ता था।
12 फरवरी 1852 को फुले दम्पत्ति द्वारा स्थापित कन्या पाठशालाओं की खुली परीक्षा आयोजित की गयी। इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में नागरिक और विशिष्ट जन उपस्थित हुये। इनमें से एक न्यायाधीश श्री ब्राउन भी थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यदि महिलाएं शिक्षित बनें तो उनके घर में सुख और उपयोगिता में बढ़ोतरी होगी। इस देश में इने गिने लोग इस दिशा में विचार कर रहे हैं और देश का उद्धार करने के लिए कड़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि फुले दम्पत्ति इस दिशा में सक्रिय हैं। इस खुली परीक्षा में बालिकाएं ही कसौटी पर खरी नहीं उतरी, यह सावित्रीबाई के कड़े परिश्रम, उनकी लगन, निष्ठा और सामाजिक प्रतिबद्धता की भी परीक्षा थी। यह इसलिये कि वे उन बालिकाओं की अध्यापिका थी।
सन् 1855 में फुले दम्पत्ति ने पुणे में रात्रि पाठशाला की स्थापना की। इस पाठशाला में दिनभर काम करने वाले मजदूरों, किसानों और गृहणियों को पढ़ाया जाता था। यह भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला थी, जिसको चलाने में सावित्रीबाई की अहम भूमिका थी।
पाठशालाओं में पढ़ने के लिये आने वाले कुछ बच्चों को जोतीराव ने अपने घर में रख लिया था। सावित्रीबाई माँ की भांति उनका पालन-पोषण करती थी।
बाद में उन्होंने एक अनाथालय खोला ताकि अनाथ बच्चों को रखा जा सके। इस काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। इसमें विधवाएं अपने बच्चों को जन्म देकर सुरक्षित छोड़ सकती थी। जोतीराव और सावित्रीबाई ही इन बच्चों के पालनहार थे।
फुले दम्पत्ति की महानता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे ही एक बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया था। इस बच्चे को पढ़ा-लिखाकर उन्होंने डॉक्टर बनाया। यही बच्चा डॉ.यशवंत कहलाया और फुले दम्पत्ति ने उसको अपनी जायदाद का उत्तराधिकारी बनाया था।
सावित्रीबाई एक आदर्श धर्म सुधारक थी। अपने पति के साथ उन्होंने सत्यशोधक समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद ही नहीं कि अपितु जोतीराव की मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का 8 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन भी किया था।
सन् 1897 में पुणे नगर में प्लेग का प्रकोप फैला तो आसपास के गाँव भी उसकी चपेट में आ गये, सावित्रीबाई घर-घर जाकर रोगियों को अपने पुत्र यशवंत के पास इलाज के लिए लाने में जुट गयी। इसी दौरान वे स्वंय भी इस रोग का शिकार हो गयी। यह पुण्य ज्योति 10 मार्च 1897 को परम पिता परमेश्वर में विलीन हो गयी। उनके निधन से सत्य एवं सेवा की एक मशाल बुझ गयी, जिसने आदमीयत को रोशन किया था।
वे एक चिन्तनशील विचारक थी। उनके विचारों की मौलिकता को उजागर करने वाला उनका एक कथन दृष्टव्य है-
‘‘दो हजार सालों से शुद्रातिशुद्रों को श्रेष्ठ लोगों ने ज्ञान, सम्पत्ति एवं राजसत्ता से अलग रखा है। बाहर से आये आर्यों ने यहां के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। मुट्ठीभर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने घमण्ड और दम्भ के कारण बाद में अकेले ही विदेशियों से लडे़, आमजन को साथ नहीं लिया। वे हम छोटों को पूछते तक नहीं थे। विदेशियों ने उन्हें जीतकर मिट्टी में मिला दिया। अतः देश की बार-बार होने वालीे पराजय के लिये वे ही जिम्मेदार हैं।’’
संक्षिप्ततः उल्लिखित सन्दर्भों में सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके संघर्ष एवं योगदान की जो तस्वीर बनती है, उसके रंग क्रांति के रंग हैं। 19 वीं सदी के सन्दर्भ में उनकी क्रांतिधर्मिता का महत्व और भी बढ़ जाता है जब नारी शोभा या उपभोग के अलावा कुछ नहीं थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में की गयी सावित्रीबाई की सेवाएँ समय के सीने पर खींची ऐसी गहरी रेखाएँ हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पगडंडी से खुली सड़क बन चुकी है। आज के सन्दर्भों में सावित्रीबाई की क्रांतिधर्मिता नारी समाज के लिए एक अनुकरणीय रास्ता है।